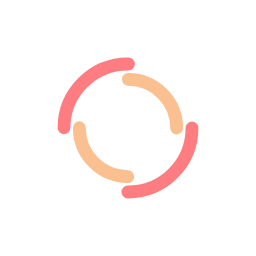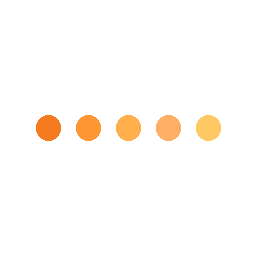Courses
Grow skills with quality courses



झूम कृषि (slash and burn farming) एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों (लकड़ी के हलों आदि) से जुताई करके बीज बो दिये जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। कुछ वर्षों तक (प्रायः दो या तीन वर्ष तक) जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात् इस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़-पौधें उग आते हैं। अब अन्यत्र जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है और उस पर भी कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है। इस प्रकार यह एक स्थानानंतरणशील कृषि (shifting cultivation) है जिसमें थोड़े-थोड़े समय के अंतर पर खेत बदलते रहते हैं। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इस प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि को श्रीलंका में चेना, हिन्देसिया में लदांग और रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं

स्थानान्तरी कृषि अथवा स्थानान्तरणीय कृषि (अंग्रेज़ी: Shifting cultivation) कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिये चुना जाता है और उपजाऊपन कम होने के बाद इसका परित्याग कर दूसरे टुकड़े को ऐसी ही कृषि के लिये चुन लिया जाता है। पहले के चुने गये टुकड़े पर वापस प्राकृतिक वनस्पति का विकास होता है। आम तौर पर १० से १२ वर्ष, और कभी कभी ४०-५० की अवधि में जमीन का पहला टुकड़ा प्राकृतिक वनस्पति से पुनः आच्छादित हो कर सफाई और कृषि के लिये तैयार हो जाता है। झूम कृषि भी एक प्रकार की स्थानान्तरी कृषि ही है। इसके पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए भारत के कुछ हिस्सों में इस पर प्रतिबन्ध भी आयद किया गया है स्थानांतरित कृषि से मृदा अपरदन तथा वनों का हास्य होता है जिस कारण प्रायः इसकी आलोचना की जाती है। फिर भी यह सबसे पुरानी कृषि पद्धति है और हजारों वर्षों से चली आ रही है। यदि यह कृषि एक निश्चित सीमा तक की जाए जिससे मृदा तथा वनस्पति प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं और परिस्थितिक तंत्र का संतुलन ना बिगड़े तो इस कृषि के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है। अतः यह विचार की स्थानांतरित केसी हर परिस्थिति में हानिकारक है न्याय संगत नहीं है। परंतु पिछले कुछ दशकों में अफ्रीका लैटिन अमेरिका तथा एशिया के स्थानांतरित कृषि वाले इलाकों में जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। इससे स्थानांतरित कृषि वाली वन्य भूमि पर भार अत्यधिक बढ़ गया है जिसे वन करने में यह प्रदेश असमर्थ हैं। स्थानांतरित कृषि एक विस्तृत कैसी है जिसमें लगभग 90% भूमि प्रति छोड़नी चाहिए ताकि मृदा और वन संपदा को सहन शक्ति से अधिक हानि न पहुंचे। परंतु तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए उन भू भागो में भी कृषि की जाने लगी है जिन्हें प्रति छोड़ देना चाहिए।इससे मृदा तथा वन संपदा की हानि होती है और मृदा की उपजाऊ शक्ति कम होती है कृषि उपज में कमी आती है। कुछ प्रदेशों में तो भूमि पूर्णतया बंजर हो जाती है और किसी के लिए स्थाई रूप से अयोग्य हो जाती है।

झूम कृषि (slash and burn farming) एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों (लकड़ी के हलों आदि) से जुताई करके बीज बो दिये जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। कुछ वर्षों तक (प्रायः दो या तीन वर्ष तक) जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात् इस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़-पौधें उग आते हैं। अब अन्यत्र जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है और उस पर भी कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है। इस प्रकार यह एक स्थानानंतरणशील कृषि (shifting cultivation) है जिसमें थोड़े-थोड़े समय के अंतर पर खेत बदलते रहते हैं। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इस प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि को श्रीलंका में चेना, हिन्देसिया में लदांग और रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं। स्थानान्तरी कृषि अथवा स्थानान्तरणीय कृषि (अंग्रेज़ी: Shifting cultivation) कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिये चुना जाता है और उपजाऊपन कम होने के बाद इसका परित्याग कर दूसरे टुकड़े को ऐसी ही कृषि के लिये चुन लिया जाता है। पहले के चुने गये टुकड़े पर वापस प्राकृतिक वनस्पति का विकास होता है। आम तौर पर १० से १२ वर्ष, और कभी कभी ४०-५० की अवधि में जमीन का पहला टुकड़ा प्राकृतिक वनस्पति से पुनः आच्छादित हो कर सफाई और कृषि के लिये तैयार हो जाता है।

Jhoom cultivation is a local name for slash and burn agriculture practiced by the tribal groups in the northeastern states of India like Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland and also in the districts of Bangladesh

फिनलैण्ड में झूम खेती के लिये वन जलाया जा रहा है।(१८९३ में ) झूम कृषि (slash and burn farming) एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों (लकड़ी के हलों आदि) से जुताई करके बीज बो दिये जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। कुछ वर्षों तक (प्रायः दो या तीन वर्ष तक) जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात् इस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़-पौधें उग आते हैं।